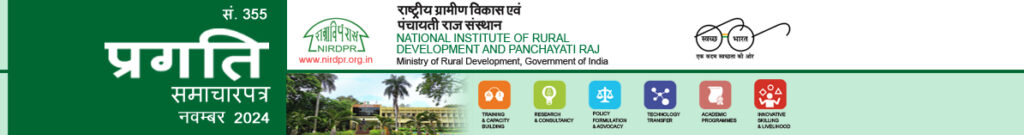
विषय सूची:
मुख्य कहानी : सामुहिक सफलता को उजागर करने वाला पेन उद्यम : एनआरईटीपी इनक्यूबेटर प्रोग्राम के साथ सागरिका मण्डल की उद्यमशीलता यात्रा का एक मामला अध्ययन
मालदीव गणराज्य के द्वीप परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और एलजीए के अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम
डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत सतत आय बढ़ाने के लिए सहभागी वाटरशेड प्रबंधन पर टीओटी कार्यक्रम
ग्रामीण विकास में परियोजना मूल्यांकन के लिए अनुसंधान पद्धति पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
आदिवासी समुदायों और आजीविका के लिए गैर-लकड़ी वन उत्पादों के सतत उपयोग पर सेमिनार
जेंडर केलिडोस्कोप: आम महिला बोलती है: एनीमिया अलर्ट
महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने किया आईआईपीएच, हैदराबाद में एक स्वास्थ्य, एक ग्रह, एक भविष्य संगोष्ठी का उद्घाटन
एनआईआरडीपीआर में यूनिकोड पर हिंदी कार्यशाला
एनआईआरडीपीआर, एनआईपीएचएम ने टॉलिक-2 अर्धवार्षिक बैठक का आयोजन किया
एनआईआरडीपीआर ने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया
सतत आजीविका के लिए महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अभिसरण के माध्यम से एनआरएम कार्यों को बढ़ावा देना
मुख्य कहानी :
सामुहिक सफलता को उजागर करने वाला पेन उद्यम : एनआरईटीपी इनक्यूबेटर प्रोग्राम के साथ सागरिका मण्डल की उद्यमशीलता यात्रा का एक मामला अध्ययन
श्री आशुतोष धामी, युवा पेशेवर, एनआरएलएमआरसी
श्री अविजित दास, कार्यक्रम प्रमुख, आईआईएम कलकत्ता इनोवेशन पार्क
डॉ ज्योति प्रकाश मोहंती, उप निदेशक, एनआरएलएमआरसी
daynrlmcellnird@gmail.com
प्रस्तावना
एनआरईटीपी इनक्यूबेटर प्रोग्राम – ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह का पहला ग्रामीण इनक्यूबेशन प्रोग्राम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) द्वारा चार राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और कर्नाटक में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। 18 महीने तक चलने वाले इस इनक्यूबेशन प्रोग्राम को आईआईएम कलकत्ता इनक्यूबेशन पार्क द्वारा संबंधित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के सहयोग से लागू किया गया था।
इस कार्यक्रम के तहत, गैर-कृषि क्षेत्रों से 150 महिला स्वामित्व वाले/नेतृत्व वाले मौजूदा विकास नैनो/सूक्ष्म-उद्यमों का चयन किया गया, जिनका वार्षिक राजस्व कम से कम 12 लाख रुपये (एसएचजी उद्यमों/सहकारी समितियों के लिए 15 लाख रुपये और जीएसटी पंजीकरण वाले बड़े उद्यमों के लिए 20 लाख रुपये) है, जिन्हें इनक्यूबेशन सहायता के लिए चैलेंज फंड राउंड के माध्यम से प्रत्येक राज्य से चुना गया था। शामिल किए गए उद्यमों को प्रशिक्षण (व्यवसाय और डोमेन), मेंटरिंग (एक मेंटर को 10 उद्यमों के लिए मैप किया गया था), और बाजार और वित्त संबंधों में सहायता प्रदान की गई।
व्यवसाय औपचारिकीकरण
150 उद्यमों में से 18 को प्रति उद्यम 15 लाख रुपये तक के पुरस्कार/अनुदान के लिए चुना गया, तथा शेष 132 उद्यमों को 5 लाख रुपये तक के अंतर-परीक्षण-मुक्त सॉफ्ट लोन दिए गए। उद्यमियों द्वारा सलाहकारों के सहयोग से तैयार किए गए बी प्लान के अनुसार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के आधार पर उद्यमों को परियोजना वित्तपोषण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
एनआरईटीपी इनक्यूबेटर कार्यक्रम के प्रभाव का एक सम्मोहक उदाहरण मेसर्स सागरिका एंटरप्राइज है – जो पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की सुश्री सागरिका मोंडल द्वारा स्थापित एक बॉल पेन निर्माण इकाई है।
सागरिका मंडल की बॉल पेन निर्माण इकाई एनआरईटीपी इनक्यूबेटर कार्यक्रम के प्रभावी हस्तक्षेपों को उजागर करती है और यह दर्शाती है कि महिलाओं की उद्यमिता किस तरह जमीनी स्तर पर समुदायों को बदल सकती है। किसान एंटरप्राइज के विकास और उपलब्धियों की जांच करके, हम समझ सकते हैं कि प्रशिक्षण, सलाह और बाजार संबंधों सहित इनक्यूबेटर के रणनीतिक समर्थन ने कैसे व्यक्तियों को सशक्त बनाया है, आर्थिक उन्नति को बढ़ावा दिया है और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है।
पृष्ठभूमि

बोइनचिबेरिया के देहाती गांव से, सुश्री सागरिका मंडल और उनके पति ने उद्यमशीलता की यात्रा शुरू की। पूर्व फैक्ट्री कर्मचारियों ने 2004 में एक सहकर्मी के सुझाव से प्रेरित होकर अपनी बॉल पेन निर्माण इकाई शुरू करने का अवसर प्राप्त किया। 2006 में बरुईपुर में प्रशिक्षण के बाद, उन्होंने अपना उद्यम शुरू किया। उन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की, 8×8-फुट के कमरे में सिर्फ़ 10,000 रुपये और एक मैनुअल मशीन से शुरुआत की। बाधाओं के बावजूद, उन्होंने दृढ़ संकल्प और सफलता की दृष्टि से प्रेरित उद्यमशीलता की यात्रा शुरू की।
व्यापार विकास
उनकी यात्रा चुनौतियों से भरी रही और अटूट समर्पण और सीखने की प्यास के साथ उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसर में बदल दिया। फैक्ट्री कर्मचारियों से लेकर दूरदर्शी नेताओं तक, उन्होंने बदलाव को अपनाया और कुछ असाधारण बनाने का मौका भुनाया ।
अपने समुदाय को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने स्थानीय महिलाओं को भर्ती किया, उन्हें रोजगार और उद्देश्य और सशक्तिकरण की भावना प्रदान की। जैसे-जैसे उनका उद्यम बढ़ता गया, कोलकाता, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और झारखंड में फैलते हुए, गुणवत्ता और नवाचार का एक निशान छोड़ते हुए उनका प्रभाव भी बढ़ता गया ।
आज, उनका एक बार मामूली उद्यम एक संपन्न उद्यम में बदल गया है, जो 1200 वर्ग फुट के कारखाने में छह स्वचालित मशीनों के साथ स्थित है। बीस लोगों की उनकी टीम, जिसमें मुख्य रूप से उभरती हुई सशक्त महिलाएँ शामिल हैं, समावेशिता और प्रगति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है ।
2022 में आईआईएम कोलकाता इनोवेशन पार्क में प्रतिष्ठित एनआरईटीपी इनक्यूबेटर प्रोग्राम के लिए चयनित, सागरिका ने अपने व्यवसाय की परिचालन जटिलताओं में गहराई से अध्ययन किया, जिससे उनकी समझ और समृद्ध हुई और उनका संकल्प मजबूत हुआ।
व्यवसाय मूल्य श्रृंखला
आतंरिक सामग्री :
पेन बॉडी, कैप और एडेप्टर जैसे कच्चे माल स्थानीय थोक विक्रेता से खरीदे जाते हैं जो कारखाने में डिलीवरी करते हैं। ये सामग्री आमतौर पर हर 15 दिन में या प्राप्त ऑर्डर की मात्रा के आधार पर खरीदी जाती है. अधिग्रहण प्रक्रिया कुशल है, इसे पूरा होने में केवल एक दिन लगता है। हालाँकि, इन लेन-देन के लिए कोई क्रेडिट सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद, कच्चे माल की उपलब्धता लगभग सुचारू बनी हुई है, जिससे उत्पादन में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित होता है ।
अन्य कच्चे माल, जैसे नोजल और स्याही, हावड़ा-बुर्राबाजार से प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें हर 15 दिन में खरीदा जाता है, और अधिग्रहण प्रक्रिया तेज़ होती है, आमतौर पर इसमें सिर्फ़ एक दिन लगता है। अन्य आपूर्तियों की तरह, इन लेन-देन के लिए कोई क्रेडिट सुविधा उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, इन सामग्रियों की उपलब्धता लगातार सुचारू है, जिससे उत्पादन के लिए एक स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित होती है ।
संचालन:
एडाप्टर फिटिंग, इंक फिलिंग, निब फिटिंग और प्रिंटिंग जैसी प्रक्रियाएं स्वचालित मशीनों द्वारा प्रबंधित की जाती हैं, जबकि सेंट्रीफ्यूगल मशीन अर्ध-स्वचालित होती है। सफाई, कैपिंग और पैकेजिंग मैन्युअल रूप से की जाती है। गुणवत्ता जांच (क्यूसी) 100 यादृच्छिक नमूनों पर की जाती है ।
बाहरी सामग्री :
तैयार माल को इन्वेंट्री में रखा जाता है और रिक्शा वैन और फिर ट्रक द्वारा थोक विक्रेताओं तक पहुँचाया जाता है। कभी-कभी, वे परिवहन/कूरियर एजेंसियों पर निर्भर होते हैं ।
विपणन और बिक्री:
उद्यमी को अभी भी विपणन और बिक्री गतिविधियाँ शुरू करने की आवश्यकता है ।
मानव संसाधन:
स्थानीय महिलाएँ दैनिक मज़दूरी के आधार पर हाथ से काम करती हैं, जिनमें से छह महिलाएँ 8 घंटे काम करके प्रतिदिन 250 रुपये कमाती हैं, और 10-12 महिलाएँ घर पर खाली समय में 120 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से काम करती हैं। पुरुष कर्मचारी मासिक वेतन के आधार पर मशीन संचालन करते हैं; दो मशीन ऑपरेटर 8000 प्रति माह कमाते हैं और प्रतिदिन 8 से 10 घंटे काम करते हैं ।
फर्म अवसंरचना:
दैनिक नकद बही और खरीद बही का रखरखाव उद्यमी द्वारा स्वयं किया जाता है। युपीआई भुगतान स्वीकार किया जाता है ।
| आधार रेखा (एफवाईई – 22-23) | अंतरेखा (एफवाईई – 23-24) | |
| वार्षिक राजस्व (रू.) | 15,840,000 | 21,325,649 |
| सकल लाभ | 475,200 | 572,650 |
| आजीविका | दैनिक वेतनभोगी (पूर्णकालिक) – 5 दैनिक वेतनभोगी (अंशकालिक) – 10 स्थायी कर्मचारी – 3 | दैनिक वेतनभोगी (पूर्णकालिक) – 6 दैनिक वेतनभोगी (अंशकालिक) – 12 स्थायी कर्मचारी – 4 |
| बाज़ार संवितरण | बी2बी: 100% बी2सी – व्यापार: 00% | बी2बी: 95% बी2सी – व्यापार : 05% |
| भौगोलिक | पश्चिम बंगाल असम दिल्ली ग्वालियर | (+)हैदराबाद (+) स्थानीय बाजार |
हस्तक्षेप सारांश:
एनआरईटीपी इनक्यूबेशन प्रोग्राम के तहत उद्यमी को बिजनेस बेसिक्स पर 64 घंटे की ट्रेनिंग मिली। उन्हें भारतीय गुणवत्ता परिषद से लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज पर ट्रेनिंग और एमएसएमई लीन कॉम्पिटिटिव स्कीम पर बेसिक लेवल सर्टिफिकेट भी मिला। उद्यम को थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर्स और कॉर्पोरेट खरीदारों से जोड़ा गया। मेंटर की सिफारिश और बिजनेस प्लान के मुताबिक, उन्होंने अपने ब्रांड नाम से प्रीमियम बॉलपॉइंट पेन बनाना शुरू किया। उद्यम को एमएसएमई उद्यम आधार सर्टिफिकेट भी मिला। फंडिंग के सहारे उन्होंने नई ऑटोमेटिक मशीन लगाकर उत्पादन क्षमता बढ़ाई ।
चुनौतियाँ और समाधान:
सुश्री सागरिका मंडल स्थानीय बाजार में अपने ब्रांड के लिए पेन लॉन्च करने और बेचने की योजना बना रही हैं। उन्होंने उत्पाद की विविधता भी बढ़ाई है। अब, वे तीन अलग-अलग प्रकार के पेन बना रही हैं। सबसे कम गुणवत्ता वाला पेन थोक विक्रेता को 1.80 रुपये प्रति पीस पर बेचा जाता है, और उत्पादन लागत 1.66 रुपये है। हाल ही में, उन्हें थोक विक्रेताओं से पेन बनाने के लिए ऑर्डर मिले हैं, जिन्हें 8 रुपये में बेचा जाएगा। उद्यमी ने 2.2 लाख रुपये की लागत वाली एक पूरी तरह से स्वचालित पेन निर्माण मशीन भी खरीदी है, जो उन्हें उत्पादन क्षमता को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने और बर्बादी को कम करके उत्पादन लागत को 5 प्रतिशत तक कम करने में मदद करेगी। सुश्री सागरिका मंडल अपने ब्रांड के लिए ट्रेडमार्क के लिए आवेदन करने के लिए कदम उठा रही हैं। भविष्य में, उद्यमी कार्य-ऑर्डर के आधार पर पेन निर्माण के मौजूदा व्यवसाय मॉडल को बदलकर केवल अपने स्वयं के ब्रांडेड पेन बनाने की योजना बना रहे हैं, और सुश्री सागरिका मंडल ने काम का प्रबंधन करने के लिए एक अलग मार्केटिंग टीम को नियुक्त करने की योजना बनाई है।

पेन निर्माण इकाई का दौरा करें
आर्थिक और सामाजिक प्रभाव
रोज़गार सृजन:
विनिर्माण इकाई की स्थापना से स्थानीय आबादी के लिए महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए, खासकर उत्पादन, पैकेजिंग, रखरखाव, गुणवत्ता नियंत्रण और वितरण जैसे क्षेत्रों में। इन पदों ने स्थानीय श्रमिकों को स्थिर नौकरियां और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए, जिससे समुदाय के भीतर आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। इसके अतिरिक्त, विनिर्माण इकाई की उपस्थिति ने परिवहन, कच्चे माल की आपूर्ति और सहायक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन कर स्थानीय अर्थव्यवस्था में एक लहर जैसी स्थिति निर्माण की है ।
आय वृद्धि और गरीबी में कमी:
विनिर्माण इकाई में नए रोजगार के अवसर शुरू करने से स्थानीय कार्यबल में बदलाव आया है, खासकर महिला श्रमिकों के लिए। रोजगार में वृद्धि के साथ, कई महिलाओं ने घरेलू आय में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जिससे उनके परिवारों के समग्र जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इस आर्थिक उत्थान ने गरीबी के स्तर को कम किया है, खासकर अकुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए जिनके पास स्थिर रोजगार तक पहुंच है ।
स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा:
इस इकाई की उपस्थिति से स्थानीय व्यवसायों को लाभ हुआ जो कारखाने को सेवाएं या सामान प्रदान करते हैं, जैसे कि कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता, रसद प्रदाता और खुदरा विक्रेता ।
महिला सशक्तिकरण:
विनिर्माण इकाई ने संग्रहण और पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों में कई महिलाओं को रोजगार दिया। इससे समुदाय में महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिली, जिससे उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक स्थिति मिली ।
निष्कर्ष
बॉल पेन निर्माण इकाई रोजगार सृजन, स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे में सुधार करके आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करती है। यद्यपि महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सहित सामाजिक प्रभाव महत्वपूर्ण है, लेकिन क्षेत्र के सतत और न्यायसंगत विकास को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन और सामुदायिक एकीकरण पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। जबकि सामाजिक और आर्थिक लाभ काफी हैं, इकाई को स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने और गांव में कृषि और मत्स्य पालन पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन और उत्सर्जन जैसे पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने की आवश्यकता होगी।
मालदीव गणराज्य के द्वीप परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और एलजीए के अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम

पंचायती राज, विकेंद्रीकृत योजना और सामाजिक सेवा वितरण केंद्र (सीपीआरडीपी और एसएसडी) ने मालदीव गणराज्य के द्वीप परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और स्थानीय सरकार प्राधिकरण (एलजीए) के अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। 24 अक्टूबर से 7 नवंबर 2024 तक आयोजित यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) और मालदीव के एलजीए के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत चल रहे सहयोग का हिस्सा था। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने इस कार्यक्रम का समर्थन किया। विभिन्न द्वीप परिषदों से नौ महिलाएँ और 19 पुरुष सहित कुल 28 प्रतिभागियों और मालदीव के एलजीए के दो अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। प्रशिक्षण एनआईआरडीपीआर के विशेषज्ञ संकाय सदस्यों द्वारा सुगम बनाया गया, जिन्होंने सतत विकास, शासन और समुदाय-संचालित पहलों के बारे में गहन ज्ञान दिया।
कार्यक्रम अवलोकन
14 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों की नेतृत्व क्षमताओं को बढ़ाना है, ताकि उन्हें अपने समुदायों के लिए नेतृत्व करने, रणनीति बनाने और नीतियां विकसित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस किया जा सके। यह पहल चार वर्षों (2022-2026) में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें एनआईआरडीपीआर ने पहले ही छह ऐसे प्रशिक्षण सत्र पूरे कर लिए हैं।
उद्घाटन सत्र
कार्यक्रम का उद्घाटन एनआईआरडीपीआर के पाठ्यक्रम निदेशक और एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख (सीपीआरडीपी एवं एसएसडी) डॉ. अंजन कुमार भँज ने किया, जिन्होंने प्रतिभागियों का स्वागत किया और प्रशिक्षण के उद्देश्यों का अवलोकन प्रदान किया। उन्होंने प्रतिनिधियों को एनआईआरडीपीआर के विभिन्न विभागों का पता लगाने और ग्रामीण विकास पद्धतियों की अपनी समझ को व्यापक बनाने के लिए संकाय सदस्यों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। एनआईआरडीपीआर के रजिस्ट्रार एवं निदेशक प्रशासन श्री मनोज कुमार ने मुख्य भाषण दिया, जिसमें स्थानीय शासन को मजबूत करने में कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला और एनआईआरडीपीआर की अत्याधुनिक शिक्षण सुविधाओं पर जोर दिया।
क्रियाविधि
प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण पद्धतियों का उपयोग किया गया, जैसे व्याख्यान और पीपीटी की सहायता से परिचर्चा सत्र, वीडियो क्लिप, लघु फिल्में, समूह गतिविधियां और चर्चाएं, तथा प्रतिदिन नियमित सत्र शुरू होने से पहले प्रतिभागियों द्वारा पुनर्कथन सत्र, जिसमें कार्यक्रम के व्यापक और विशिष्ट उद्देश्यों, अवधि और प्रतिभागियों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखा गया।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न संबंधित पहलुओं को शामिल किया गया, जैसे.,
- भारत में पहल और अच्छे व्यवहारों के संदर्भ में द्वीप परिषदों में विकेन्द्रीकृत योजना के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की गुंजाइश की आवश्यकता
- द्वीप परिषदों के सदस्यों के बीच नेतृत्व को बढ़ावा देना
- मालदीव के संदर्भ में सौर प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की गुंजाइश
- ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) सहित कुछ अच्छे अभ्यासों के आधार पर मालदीव में नवीन और उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्योगिकी के अनुकरण की गुंजाइश
- भारत की प्रणालियों के संदर्भ में मालदीव के द्वीप परिषदों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में विकसित करने की परिकल्पना
- भारत में अच्छे अभ्यासों के आधार पर मालदीव में मत्स्य पालन क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश
- भारत में एनआरएलएम के लक्ष्य और मुख्य विशेषताएं तथा द्वीप परिषदों के राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण की संभावनाएं
- भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सर्वोत्तम अभ्यास
- मालदीव में आर्थिक विकास के लिए कौशल विकास की संभावनाएं
- भारत में अच्छी पद्धतियों के आधार पर मालदीव में कृषि, बागवानी और पुष्प-कृषि क्षेत्रों में सुधार की संभावनाएं
- चारमीनार, गोलकुंडा (हैदराबाद में सांस्कृतिक विरासत) का स्थानीय दौरा
- सार्वजनिक सेवा वितरण में समुदाय के नेतृत्व वाली जवाबदेही और पारदर्शिता (सामुदायिक स्कोर कार्ड)
- पंचायतों के माध्यम से सेवा वितरण की स्थिति में सुधार की गुंजाइश
- भारत में अच्छे व्यवहारों के संदर्भ में स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) के माध्यम से द्वीप परिषदों के वित्त को मजबूत करना
क्षेत्र का दौरा
प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र दौरा था, जिसने प्रतिभागियों को विभिन्न समुदाय-संचालित विकास पहलों के बारे में व्यावहारिक जानकारी प्रदान की। इस यात्रा में कई ज्ञानवर्धक पड़ाव शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक ने ग्रामीण शासन और विकास के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला:

- एस आर पुरम गांव: प्रतिभागियों ने पेंडुर्थी मंडल के एक गांव एस आर पुरम का दौरा किया, जहां उन्होंने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों से बातचीत की। ये समूह, मुख्य रूप से महिलाओं से संबंधित हैं, बचत और उधार के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता और स्वास्थ्य जागरूकता और साक्षरता अभियान जैसी सामाजिक पहलों के माध्यम से सामुदायिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रतिभागियों ने यह भी देखा कि कैसे एसएचजी को सरकारी योजनाओं और गैर सरकारी संगठनों द्वारा समर्थन दिया जाता है, जिससे महिला सशक्तिकरण और आर्थिक उत्थान को बढ़ावा मिलता है ।
- अराकू में डीडीयू-जीकेवाई स्किल कॉलेज: इस यात्रा में व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया गया
- ग्राम स्वास्थ्य केंद्र और ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई: स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में, प्रतिभागियों ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी के बारे में सीखा, जिसमें स्वास्थ्य शिविरों और टीकाकरण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। उन्होंने गांव के ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र का भी दौरा किया, और देखा कि कैसे समुदाय द्वारा संचालित पहल प्रभावी रूप से अपशिष्ट का प्रबंधन करती है।
- एस आर पुरम ग्राम पंचायत कार्यालय: प्रतिभागियों ने एस आर पुरम में ग्राम पंचायत (ग्राम सचिवालय) कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय सरकार के कामकाज को समझने के लिए सरपंच, वार्ड सदस्यों, पंचायत सचिव और लाइन विभाग के अधिकारियों से बातचीत की। चर्चाओं में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन निर्माण की अनुमति, जल आपूर्ति प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण नागरिक सेवाओं और पेंशन और छात्रवृत्ति जैसी सामाजिक कल्याण योजनाओं पर चर्चा की गई।
- मंडल परिषद (ब्लॉक पंचायत): प्रतिभागियों ने मंडल परिषद कार्यालय का भी दौरा किया, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों पर चर्चा की। इस दौरे से उन्हें ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक ढांचे और स्थानीय शासन के कामकाज की बेहतर समझ मिली ।
- जिला कलेक्टर कार्यालय: अध्ययन दौरे में जिला कलेक्टर के कार्यालय का दौरा भी शामिल था, जहाँ विशाखापट्टनम के जिला कलेक्टर श्री एम एन हरेंधीरा प्रसाद, आईएएस ने जिला-स्तरीय प्रशासन और शासन रणनीतियों पर जानकारी साझा की। उन्होंने मालदीव के प्रशासनिक ढांचे के बारे में भी जानकारी ली और इस बात पर चर्चा की कि प्रतिभागी प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान को अपने देश में कैसे लागू कर सकते हैं।
इन यात्राओं से बहुमूल्य शिक्षण के अवसर प्राप्त हुए, तथा प्रतिभागियों को शासन, ग्रामीण विकास, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं आदि पर व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ।
एक्सपोजर विजिट: भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, सौर और पवन प्रौद्योगिकी, ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी), राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी)
परिणाम और प्रतिक्रिया
प्रशिक्षण कार्यक्रम ने प्रतिभागियों की शासन व्यवस्था, सार्वजनिक सेवा वितरण, वित्तीय प्रबंधन और सामुदायिक विकास की समझ को सफलतापूर्वक बढ़ाया। प्रतिभागियों ने विशेष रूप से विकेंद्रीकृत नियोजन, नेतृत्व और संधारणीय पद्धतियों के अनुप्रयोग पर प्राप्त व्यावहारिक अंतर्दृष्टि की सराहना की। उन्होंने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत करने और ग्रामीण विकास, अपशिष्ट प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा में सफल मॉडलों से सीखने के अवसर के लिए आभार भी व्यक्त किया ।
प्रतिभागियों से प्राप्त फीडबैक में कार्यक्रम की सुव्यवस्थित संरचना, उनके काम के लिए इसकी प्रासंगिकता और इंटरैक्टिव तथा सहभागी प्रशिक्षण विधियों के प्रभावी उपयोग पर प्रकाश डाला गया। एनआईआरडीपीआर द्वारा प्रदान किए गए शांत वातावरण, उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे और आतिथ्य की भी प्रशिक्षण की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कारकों के रूप में प्रशंसा की गई।
कार्यक्रम का नेतृत्व और समन्वय डॉ. अंजन कुमार भँज ने किया, जिसमें प्रशिक्षण प्रबंधक के रूप में सुश्री ए. सिरिशा और श्री अरुण राज माली का सहयोग रहा।
फोटो गैलरी
डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत सतत आय बढ़ाने के लिए सहभागी वाटरशेड प्रबंधन पर टीओटी कार्यक्रम

सीसी एंड डीएम के साथ प्रतिभागियों की समूह फोटो
सतत कृषि पद्धतियों के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) ने 26 से 29 नवंबर 2024 तक ‘डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत सतत आय बढ़ाने के लिए सहभागी जलागम प्रबंधन’ पर एक व्यापक चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) 2.0 के तहत भागीदारी वाटरशेड प्रबंधन पद्धतियों की समझ को गहरा करने के लिए राज्य के अधिकारियों, गैर सरकारी प्रतिनिधियों और भारत भर के विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया, जिसमें जल विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) पर ध्यान केंद्रित किया गया।

प्रशिक्षण में 12 राज्यों के 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो जल संसाधन, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, मृदा संरक्षण और गैर सरकारी संगठनों जैसे विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व करते थे। चार दिनों के दौरान, उन्हें कृषि उत्पादकता बढ़ाने, जल संसाधन प्रबंधन में सुधार करने और ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय-संचालित विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थायी वाटरशेड प्रबंधन पद्धतियों को लागू करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस किया गया।
कार्यक्रम के उद्देश्य और लक्ष्य
प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्राथमिक लक्ष्य थे:
- तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ाना: पीएमकेएसवाई 2.0 के प्रभावी कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए सहभागी वाटरशेड प्रबंधन में विशेष ज्ञान वाले लाइन विभागों के अधिकारियों की क्षमता को मजबूत करना।
- सहयोग को बढ़ावा देना: विभिन्न लाइन विभागों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, प्रतिभागियों को ज्ञान साझा करने, विभिन्न वाटरशेड प्रबंधन रणनीतियों को एकीकृत करने और सतत जल और भूमि संसाधन प्रबंधन के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण की दिशा में काम करने में सक्षम बनाना।
- नीति अनुप्रयोग और कार्यान्वयन: सहभागी जलग्रहण प्रबंधन के संदर्भ में विभागीय नीतियों और दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिभागियों को उपकरणों से लैस करना, ग्रामीण विकास और जल संसाधन संरक्षण के व्यापक उद्देश्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करना ।
सत्रों का दिनवार विवरण
कार्यक्रम की शुरुआत एनआईआरडीपीआर में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन केंद्र (सीएनआरएम) के प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. रवींद्र एस. गवली के उद्घाटन सत्र से हुई, जिन्होंने कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए वाटरशेड प्रबंधन में नवीन तकनीकों के महत्व पर जोर दिया। सहायक प्रोफेसर और कार्यक्रम निदेशक डॉ. राज कुमार पम्मी ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत भागीदारी रणनीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अधिकारियों की क्षमता निर्माण में प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला।
पहले तकनीकी सत्र में अद्यतन डब्ल्यूडीसी – पीएमकेएसवाई 2.0 ढांचे का अवलोकन किया गया, जिसमें वाटरशेड प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी के महत्व और सतत जल और भूमि उपयोग पद्धतियों को प्राप्त करने की रणनीतियों को शामिल किया गया। डॉ. राज कुमार पम्मी ने कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों पर गहराई से जानकारी दी, जबकि डॉ. गवली ने फसल जल बजट की अवधारणा और कुशल जल उपयोग सुनिश्चित करने में इसके महत्व को प्रस्तुत किया।
बाद में, प्रतिभागियों ने आईसीएआर-भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) में न्यूट्री-हब इनक्यूबेशन सेंटर का दौरा किया, जहाँ उन्होंने बाजरा आधारित उत्पादों के पोषण मूल्य और बाजार क्षमता को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नवीन तकनीकों का पता लगाया। बाजरा आधारित कृषि पद्धतियों के इस प्रदर्शन ने प्रतिभागियों को निरंतर खेती और ग्रामीण आजीविका को बेहतर बनाने में मूल्यवर्धित उत्पादों की भूमिका के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी।
तीसरे दिन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अभिसरण और सफल जलग्रहण प्रबंधन के लिए उनका लाभ कैसे उठाया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। डॉ. राज कुमार पम्मी ने कार्यक्रम अभिसरण के औचित्य पर एक सत्र का नेतृत्व किया, जिसमें ग्रामीण विकास पर उनके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए एमजीएनआरईजीए (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना), पीएमकेएसवाई और अन्य सरकारी कार्यों जैसी विभिन्न योजनाओं को एकीकृत करने के महत्व पर जोर दिया गया।
एनआईआरडीपीआर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. केशव राव ने डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के भीतर तर्कसंगत भूमि और जल उपयोग के लिए जीआईएस-आधारित योजना पर एक सत्र आयोजित किया। वाटरशेड प्रबंधन में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के उपयोग को सतत योजना, वाटरशेड परिसीमन और परियोजना परिणामों की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उजागर किया गया। प्रतिभागियों ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वित अंतर-विभागीय सहयोग और अभिनव वाटरशेड प्रबंधन रणनीतियों के सफल उदाहरणों को प्रदर्शित करते हुए राज्य-स्तरीय मामला अध्ययन भी साझा किया।
अंतिम दिन मौसम आधारित कृषि सलाह और एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सीआरआईडीए (केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान) के डॉ एएमवी सुब्बा राव ने कृषि निर्णय लेने में मौसम पूर्वानुमान के महत्व पर चर्चा की और ऐसे मामला अध्ययन साझा किए, जो मौसम आधारित सलाह का पालन करने के आर्थिक लाभों को प्रदर्शित करते हैं। सीआरआईडीए के प्रधान वैज्ञानिक डॉ मोहम्मद उस्मान ने प्रतिभागियों को विभिन्न आईएफएस मॉडल, जैसे फसल-डेयरी, फसल-पशुधन और कृषि वानिकी से परिचित कराया, जिन्हें आय बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए वाटरशेड क्षेत्रों में एकीकृत किया जा सकता है।
समापन सत्र में डॉ. राज कुमार पम्मी ने प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए। उन्होंने जमीनी स्तर पर वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए प्राप्त ज्ञान को लागू करने के महत्व पर जोर दिया। सत्र के दौरान एकत्र किए गए प्रतिभागियों के फीडबैक ने उच्च संतुष्टि का संकेत दिया, जिसमें कार्यक्रम की प्रभावशीलता, प्रासंगिकता और परिचर्चात्मक प्रकृति के लिए 90 प्रतिशत की समग्र रेटिंग थी।
क्षेत्रीय दौरे और व्यावहारिक शिक्षा
प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्षेत्रीय दौरे भी शामिल थे, जिससे प्रतिभागियों को वास्तविक दुनिया में वाटरशेड प्रबंधन तकनीकों के व्यावहारिक अनुप्रयोग को देखने का अवसर मिला।

अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में फसलों पर केंद्रित विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त शोध संस्थान आईसीआरआईएसएटी के दौरे से प्रतिभागियों को कंटूर बंडिंग, वर्षा जल संचयन और चेक डैम के निर्माण जैसे स्थायी जल प्रबंधन पद्धतियों के प्रभावों को प्रत्यक्ष रूप से देखने का मौका मिला। जल अपवाह को कम करने और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये उपाय जल की कमी वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए आवश्यक थे। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदाय के सदस्यों के साथ चर्चा की, जल संसाधनों के प्रबंधन में उनके अनुभवों और ऐसे कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने में सामूहिक कार्रवाई के महत्व के बारे में जाना।
इस यात्रा का एक मुख्य आकर्षण वाटरशेड प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी का प्रदर्शन था। प्रतिभागियों ने देखा कि कैसे स्थानीय किसान और समुदाय के सदस्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी ज़रूरतों और चिंताओं को नियोजन और कार्यान्वयन चरणों में संबोधित किया गया था। सहभागी दृष्टिकोणों के इस प्रदर्शन ने वाटरशेड प्रबंधन पद्धतियों का स्वामित्व लेने के लिए समुदायों को सशक्त बनाने पर प्रशिक्षण के मुख्य फोकस को मजबूत किया
आईसीएआर-भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) में न्यूट्री-हब इनक्यूबेशन सेंटर के दोपहर के दौरे ने प्रतिभागियों को अभिनव कृषि पद्धतियों से परिचित कराया, जो अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण सूखा-प्रतिरोधी फसल बाजरा के पोषण मूल्य और बाजार क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। बाजरा से मूल्यवर्धित उत्पादों पर केंद्र का ध्यान ग्रामीण किसानों के लिए आय स्रोतों में विविधता लाने का एक मॉडल पेश करता है। कृषि नवाचार को वाटरशेड प्रबंधन के साथ एकीकृत करके, कार्यक्रम ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे सतत भूमि और जल पद्धतियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तीकरण में भी योगदान दे सकती हैं।

इन यात्राओं के दौरान व्यावहारिक शिक्षा प्रतिभागियों के लिए सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक अनुप्रयोगों से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण थी। इन क्षेत्र-आधारित अनुभवों ने प्रतिभागियों को वाटरशेड प्रबंधन की जटिलताओं के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की और उन्हें ग्रामीण विकास परियोजनाओं की बहुआयामी प्रकृति को समझने में मदद की, जिसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की आवश्यकता होती है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम एक शानदार सफलता साबित हुआ, जिसमें प्रतिभागियों को स्थायी जलग्रहण प्रबंधन, जलवायु-लचीली कृषि पद्धतियों और जल संसाधन संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी के महत्व के बारे में गहन ज्ञान और व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। अधिकारियों को आवश्यक कौशल से लैस करके और अंतर-विभागीय सहयोग को बढ़ावा देकर, कार्यक्रम ने भारत भर में भागीदारी जलग्रहण प्रबंधन रणनीतियों के कार्यान्वयन को प्रभावित किया, जिससे डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0ढांचे के तहत कृषि उत्पादकता में वृद्धि और ग्रामीण आजीविका में सुधार हुआ।
ग्रामीण विकास में परियोजना मूल्यांकन के लिए अनुसंधान पद्धति पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
एनआईआरडी-पीआर के दिल्ली शाखा कार्यालय ने 04 से 08 नवंबर 2024 तक दिल्ली शाखा कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में ‘ग्रामीण विकास में परियोजना मूल्यांकन के लिए अनुसंधान पद्धति’ पर 5 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में भारत भर के आठ राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक क्षेत्र और सरकारी अधिकारियों के प्रतिभागी शामिल हुए।
कार्यक्रम का उद्घाटन सहायक प्रोफेसर डॉ. रुचिरा भट्टाचार्य के स्वागत भाषण से हुआ। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम का अवलोकन प्रस्तुत किया, ग्रामीण विकास और सीएसआर के लिए इसकी प्रासंगिकता पर जोर दिया, तथा शोध और डिजाइन के मूल सिद्धांतों पर भी प्रकाश डाला। उद्घाटन सत्र के दौरान मार्केटिंग के सहायक निदेशक श्री चिरंजी लाल भी मौजूद थे।

एस.एम. सहगल फाउंडेशन की डॉ. नीति सक्सेना ने ‘ग्रामीण विकास के लिए परियोजना मूल्यांकन प्रस्ताव तैयार करना’ और ‘परियोजना विकास एवं मूल्यांकन योजना: परिवर्तन का सिद्धांत और निगरानी ढांचा तैयार करना’ विषयों पर सत्र लिए। उन्होंने परियोजना विकास के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि आरंभ, योजना, डिजाइन, क्रियान्वयन, प्रबंधन आदि और निगरानी ढांचे के घटकों पर विभिन्न उदाहरणों की मदद से ध्यान केंद्रित किया, जिसे प्रतिभागियों ने बहुत उपयोगी पाया।

दोपहर के भोजन के बाद के सत्र के दौरान, अभ्यास और उदाहरणों की मदद से, डॉ. रुचिरा भट्टाचार्य ने प्रतिभागियों को प्रस्ताव की विषय-वस्तु से परिचित कराया, जैसे कि समस्या की पहचान, हितधारकों, मूल्यांकन प्रक्रिया और अन्य।
दूसरे दिन, एनआईआरडीपीआर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. पार्थ प्रतिम साहू ने डेटा के मूल सिद्धांतों पर सत्र लिया, डेटा के स्रोतों के बारे में जानकारी दी और विभिन्न उदाहरणों की मदद से उन्हें रूपांतरित और विश्लेषित किया।
डॉ. रुचिरा भट्टाचार्य ने दोपहर के भोजन के बाद का सत्र लिया, जिसमें उन्होंने उदाहरणों और अभ्यासों की मदद से शोध और शोध डिजाइन तथा तार्किक रूपरेखा विश्लेषण को परिभाषित किया।

तीसरे दिन, यूनिसेफ के निगरानी एवं मूल्यांकन सलाहकार डॉ. राकेश मिश्रा ने नमूनाकरण का परिचय, नमूनाकरण के प्रकार और अनुप्रयोग पर सत्र लिया, जिसमें प्रतिभागियों ने विभिन्न उदाहरणों और अभ्यासों की मदद से नमूनाकरण के मूल सिद्धांतों के बारे में सीखा।
तीसरे दिन दोपहर के भोजन के बाद के सत्र का संचालन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ट्रस्ट की निदेशक डॉ. जाह्नवी अंधारिया ने परियोजना मूल्यांकन योजना में जेंडर लेंस के उपयोग पर किया। उन्होंने प्रतिभागियों को लैंगिक समानता सातत्य को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित मूल्यांकन योजना की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उसके बाद अभ्यास और चर्चा पर एक संवादात्मक और खुला सत्र आयोजित किया गया।
चौथे दिन, डब्ल्यूआरआई के शोध, डेटा और प्रभाव टीम के प्रमुख डॉ. शमिंद्र नाथ रॉय ने मूल्यांकन के लिए मिश्रित विधि अनुसंधान के उपयोग पर एक सत्र लिया। प्रतिभागियों ने मिश्रित शोध विधि, इसके विश्लेषण और इसकी चुनौतियों के बारे में सीखा।
पॉपुलेशन काउंसिल कंसल्टिंग में कार्यनिष्पादन निगरानी विशेषज्ञ डॉ. अरूप कुमार दास ने चौथे दिन दूसरे और तीसरे सत्र का संचालन किया। उन्होंने एकतरफा और बहुभिन्नरूपी विश्लेषणों का एक व्यावहारिक परिचय दिया, तथा परियोजना मूल्यांकन में उनके अनुप्रयोगों पर प्रकाश डाला। सत्रों में प्रतिभागियों की डेटा का प्रभावी ढंग से विश्लेषण और व्याख्या करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यावहारिक आदि अभ्यास शामिल थे।

चौथे दिन चाय के बाद जेएनयू के वरिष्ठ भू-स्थानिक विशेषज्ञ डॉ. राकेश आर्य ने मूल्यांकन के लिए स्थानिक विश्लेषण पर सत्र लिया। उन्होंने हमें जीआईएस और रिमोट सेंसिंग की मूल बातें और जीआईएस में नवीनतम रुझानों के बारे में जानकारी दी, जिसमें ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न तरीके, उदाहरण और दृष्टिकोण शामिल हैं।
कार्यक्रम के पांचवें दिन, डॉ. रुचिरा भट्टाचार्य ने प्रतिभागियों के समूहों को व्यावहारिक परियोजना मूल्यांकन प्रस्तावों के लिए विशिष्ट विषय देकर प्रतिभागियों की सीख का सारांश प्रस्तुत किया, जिस पर समूहों ने प्रस्तुतियां दीं।
प्रतिक्रिया

प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की सराहना की और इसे सीखने के दृष्टिकोण से सहायक बताया । प्रतिभागियों की समग्र प्रतिक्रिया 88 प्रतिशत दर्ज की गई, जिसमें पाठ्यक्रम सामग्री के लिए 91 प्रतिशत, पठन सामग्री के लिए 80 प्रतिशत और ज्ञान प्राप्ति के लिए 97 प्रतिशत शामिल थे।
कार्यक्रम का समापन डॉ. रुचिरा भट्टाचार्य के धन्यवाद ज्ञापन और प्रमाण पत्र वितरण के साथ हुआ।
आदिवासी समुदायों और आजीविका के लिए गैर-लकड़ी वन उत्पादों के सतत उपयोग पर सेमिनार

भारत में गैर-लकड़ी वन उत्पाद (एनटीएफपी) लाखों लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर वन क्षेत्रों में और उसके आसपास के लोगों के जीवन में। ये उत्पाद, जो जंगलों से प्राप्त होते हैं, लेकिन लकड़ी को शामिल नहीं करते हैं, स्थानीय समुदायों की भलाई में योगदान करते हैं। औषधीय पौधे, मसाले, फल, मेवे, रेजिन, गोंद और रेशे जैसे एनटीएफपी के भोजन और दवा से लेकर हस्तशिल्प और औद्योगिक सामग्री तक विविध उपयोग हैं। उनकी प्रचुरता भारत की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती है। एनटीएफपी ग्रामीण समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण आय स्रोत हैं क्योंकि उनका संग्रह, प्रसंस्करण और व्यापार रोजगार और आर्थिक कल्याण प्रदान करते हैं। इसलिए, दीर्घकालिक लाभों के लिए एनटीएफपी का स्थायी प्रबंधन आवश्यक है।
कई एनटीएफपी स्वदेशी समुदायों के लिए सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व रखते हैं, और वे स्थानीय रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों का अभिन्न अंग हैं। उनके महत्व के बावजूद, एनटीएफपी को अत्यधिक दोहन और आवास क्षरण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक जरूरतों को संरक्षण के साथ संतुलित करना उनकी दीर्घकालिक उपलब्धता के लिए महत्वपूर्ण है। उचित रूप से प्रबंधित, एनटीएफपी गरीबी को काफी हद तक कम कर सकते हैं और ग्रामीण विकास में योगदान दे सकते हैं, खासकर आदिवासी समुदायों के लिए। इस संदर्भ में, एनआईआरडीपीआर ने एस.आर. शंकरन चेयर (ग्रामीण श्रम) के तहत 7-8 नवंबर 2024 को आदिवासी समुदायों और आजीविका के लिए गैर-लकड़ी वन उत्पादों (एनटीएफपी) के सतत उपयोग पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की, जिसमें आठ राज्यों के प्रतिभागी शामिल हुए। प्रतिभागियों में शिक्षाविद, व्यवसायी, सरकारी अधिकारी, छात्र और शोध विद्वान सहित विभिन्न विषयों से संबंधित थे।

दो दिनों में 22 पूर्ण शोधपत्र प्रस्तुत किए गए और उन पर चर्चा की गई, जिनकी समीक्षा की गई और एक समिति द्वारा उन्हें सूचीबद्ध किया गया। सेमिनार के शोधपत्र छह अलग-अलग तकनीकी सत्रों में प्रस्तुत किए गए, जिन्हें तीन व्यापक विषयों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया: – (क) स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के लाभ के लिए वन उत्पादों को इकट्ठा करने, प्रसंस्करण और विपणन में विविध अभ्यास; (ख) आदिवासी समुदायों के बीच आजीविका बढ़ाने के लिए मूल्यवर्धित उत्पादों को बढ़ावा देने में सूक्ष्म उद्यमों की भूमिका; और (ग) आदिवासी समुदायों के लाभ के लिए एनटीएफपी के उपयोग को बढ़ावा देने में विकास संस्थानों और स्थानीय स्वशासन का योगदान।
डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने एक व्याख्यान दिया और प्रतिभागियों से बातचीत की। उन्होंने सामान्य रूप से आदिवासी विकास और विशेष रूप से एनटीएफपी से संबंधित मुद्दों की एक पूरी श्रृंखला को सामने रखा। अपने संबोधन में, उन्होंने सतत एनटीएफपी विकास, एनटीएफपी पर वैश्विक ध्यान और जुड़ाव, विपणन चुनौतियों और समाधानों, शासन और नियामक ढांचे, संग्राहकों के लिए सुरक्षा जोखिम, स्वदेशी ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) का महत्व, लिंग की भूमिका, एनटीएफपी पर भविष्य के शोध मुद्दों के लिए रणनीतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने 3-4 मार्च 2022 को एनआईआरडीपीआर में आयोजित ‘ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बांस क्षेत्र में नवाचारों के प्रसार’ पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रमुख सिफारिशों को भी साझा किया। उन्होंने कलेक्टरों, लाइन विभागों, वन विभाग, पंचायती राज विभाग आदि के अधिकारियों सहित एनटीएफपी के विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता पर चर्चा की। महानिदेशक ने आदिवासी समुदाय के लिए सामाजिक सुरक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। उनके व्यापक विचार-विमर्श ने संगोष्ठी को बहुत जरूरी विश्वसनीयता प्रदान की।

सेमिनार ने गुणात्मक और मात्रात्मक शोध उपकरणों और पद्धतियों, मामला अध्ययनों, व्यवस्थित साहित्य समीक्षा, आख्यानों आदि पर आधारित विभिन्न शोधपत्रों को प्रस्तुत करने और चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया। प्रत्येक सत्र के बाद विस्तृत चर्चा और बातचीत हुई। एनआईआरडीपीआर के संकाय सदस्यों ने विभिन्न सत्रों की अध्यक्षता की और अवलोकन और प्रश्न साझा किए।
इस सेमिनार का समन्वयन डॉ. ज्योतिस सत्यपालन, एस.आर. शंकरन चेयर प्रोफेसर और डॉ. पार्थ प्रतिम साहू, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस (सीजीजीपीए), एनआईआरडीपीआर ने संयुक्त रूप से किया। श्री ई.बी. उदय भास्कर रेड्डी, अकादमिक एसोसिएट, सीपीजीएसएंडडीई, एनआईआरडीपीआर ने सेमिनार का समन्वयन किया।

डॉ. वानिश्री जोसेफ
प्रमुख, जेंडर अध्ययन एवं विकास केंद्र, एनआईआरडीपीआर

भारत में महिलाओं और लड़कियों में एनीमिया एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बनी हुई है। 2019 और 2021 के बीच किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5) के अनुसार, प्रचलन दरें इस प्रकार हैं:
- 6-59 महीने की आयु के बच्चे: 67.1% एनीमिया से पीड़ित हैं।
- 15-19 वर्ष की आयु की किशोर लड़कियाँ: 59.1% एनीमिया से पीड़ित हैं।
- प्रजनन आयु (15-49 वर्ष) की महिलाएँ: 57.0% एनीमिया से पीड़ित हैं।
- 15-49 वर्ष की आयु की गर्भवती महिलाएँ: 52.2% एनीमिया से पीड़ित हैं।
ये आंकड़े पिछले सर्वेक्षणों की तुलना में एनीमिया के प्रसार में वृद्धि दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, किशोर लड़कियों में एनीमिया 2015-2016 में 54% से बढ़कर 2019-2021 में 59% हो गया।
भारतीय महिलाओं और लड़कियों में एनीमिया की उच्च व्यापकता के लिए पोषण संबंधी कमियों, विशेष रूप से आयरन की कमी, अपर्याप्त आहार सेवन और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच जैसे कारकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस मुद्दे को संबोधित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनीमिया से स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं, जिसमें संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास में कमी, उत्पादकता में कमी और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वृद्धि शामिल है।
एनीमिया से निपटने के लिए, भारत सरकार ने एनीमिया मुक्त भारत (एनीमिया-मुक्त भारत) रणनीति जैसी पहलों को लागू किया है, जिसका उद्देश्य आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, आहार विविधीकरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से एनीमिया के प्रसार को कम करना है। इन प्रयासों के बावजूद, महिलाओं और लड़कियों में लगातार उच्च एनीमिया दर पोषण की स्थिति और समग्र स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन के साथ-साथ निरंतर लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता को उजागर करती है।
महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने किया आईआईपीएच, हैदराबाद में एक स्वास्थ्य, एक ग्रह, एक भविष्य संगोष्ठी का उद्घाटन
3 नवंबर 2024 को विश्व एक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में, आईआईपीएच, हैदराबाद में डॉ. साइरस पूनावाला संक्रामक रोग और महामारी तैयारी केंद्र ने 5 नवंबर, 2024 को ‘एक ग्रह, एक स्वास्थ्य, एक भविष्य’ शीर्षक से संगोष्ठी का आयोजन किया। एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक, आईएएस, डॉ जी नरेंद्र कुमार ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और एनआईआरडीपीआर की सहायक प्रोफेसर डॉ सुचरिता पुजारी ने पैनलिस्ट के रूप में ‘एक स्वास्थ्य पहल में सामुदायिक जुड़ाव’ पर एक सत्र में भाग लिया।
इस कार्यक्रम में ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिसेफ, एनआईआरडीपीआर, बिट्स पिलानी, पीवीएनआरटीवीयू, आईएमटी हैदराबाद और सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हुए। संगोष्ठी में वन हेल्थ दृष्टिकोण के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों पर चर्चा की गई, जिसमें मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के परस्पर संबंध पर जोर दिया गया।

संगोष्ठी की शुरुआत एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस के एक ज्ञानवर्धक उद्घाटन भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने कोविड-19 महामारी से सीखे गए सबक पर प्रकाश डाला और भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए शहरी और ग्रामीण समुदायों को तैयार करने के महत्व पर जोर दिया। प्रतिष्ठित वक्ताओं और पैनलिस्टों ने चर्चा की कि कैसे मानवीय गतिविधियाँ, जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण अभूतपूर्व वैश्विक स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं।
प्रमुख पैनल चर्चाएँ: वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान
संगोष्ठी में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों के नेतृत्व में पैनल चर्चा हुई, जिनमें उभरते संक्रामक रोग, रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर), खाद्य सुरक्षा और वन हेल्थ एजेंडा को आगे बढ़ाने में सामुदायिक सहभागिता की भूमिका शामिल थी।
1. वन हेल्थ रिसर्च के लिए नवीन दृष्टिकोण
बिट्स पिलानी, हैदराबाद से प्रो. पी. योगीश्वरी की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र में आईआईपीएच-एच से प्रो. रघुपति अंचला, ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी से डॉ. रुद्र गौड़ा सी और आईआईपीएच-एच से सुश्री सुभाषिनी एस जैसे विशेषज्ञ शामिल हुए। पैनल ने विभिन्न क्षेत्रों में वन हेल्थ को लागू करने की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया। मुख्य चर्चाओं में वास्तविक समय डेटा साझा करने, सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए रोगज़नक़ वैज्ञानिकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का महत्व शामिल था। वैश्विक स्वास्थ्य जोखिमों को संबोधित करने में वन हेल्थ को एक कार्यात्मक, एकीकृत अवधारणा बनाने के लिए ये दृष्टिकोण आवश्यक हैं।

2. उभरते संक्रामक रोग: एक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य
चेन्नई के सिमेट्स के डॉ. रमन मुथुसामी की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र में एनपीसीसीएचएच, तेलंगाना सरकार की डॉ. सुमित्रा नायर, ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी के डॉ. सुनील मोरे और आईआईपीएच-एच के डॉ. सिरशेंदु चौधरी शामिल थे। पैनल ने कोविड-19 के प्रमुख उदाहरण के रूप में रोग संचरण की वैश्विक अंतर्संबंधता पर जोर दिया। स्वास्थ्य कर्मियों के बीच क्षमता निर्माण और ग्रामीण आबादी को जूनोटिक रोगों के प्रकोप और निगरानी का प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया गया। चर्चा में रोग निगरानी और प्रतिक्रिया के लिए वैश्विक नेटवर्क बनाने के महत्व को रेखांकित किया गया।
3. मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को एकीकृत करना
पीवीएनआरटीवीयू के प्रो. बी. एकंबरम की अध्यक्षता में आयोजित इस पैनल में आईआईपीएच-एच के प्रो. राजन शुक्ला, यूनिसेफ के डॉ. श्रीधर प्रहलाद रयावंकी और आईआईपीएच-एच की डॉ. निरुपमा एवाई शामिल थीं। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए मानव और पशु स्वास्थ्य को एकीकृत करने पर चर्चा की। जलवायु परिवर्तन बच्चों के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, इस पर विशेष ध्यान दिया गया और पैनलिस्टों ने कमज़ोर आबादी की रक्षा के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ सहयोग की वकालत की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मनुष्य, पशु और पर्यावरण का स्वास्थ्य किस तरह से आपस में जुड़ा हुआ है और इस बात पर ज़ोर दिया कि एकीकृत दृष्टिकोण स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने और समग्र कल्याण में सुधार करने में मदद कर सकते हैं।
4. खाद्य सुरक्षा और संरक्षा: मानव और पशु स्वास्थ्य के बीच सेतु
हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रो. नंद किशोर कन्नूरी की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र में पीवीएनआरटीवीयू के प्रो. बी. एकंबरम, आईआईपीएच-एच के प्रो. जेके लक्ष्मी और आईआईपीएच-एच के प्रो. गौरी अय्यर शामिल थे। चर्चा टिकाऊ, संसाधन-कुशल खाद्य उत्पादन विधियों और खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य परिणामों को बढ़ाने की उनकी क्षमता पर केंद्रित थी। पैनलिस्टों ने तर्क दिया कि खाद्य उत्पादन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण जो मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर विचार करते हैं, तेजी से बदलती दुनिया में खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने जूनोटिक बीमारी के प्रसार को रोकने में खाद्य सुरक्षा की भूमिका पर भी जोर दिया।
5. एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर): एक वैश्विक चुनौती
आईआईपीएच-एच के प्रो. अनिल कौल की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र में ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रो. अखिलेश रामचंद्रन, आईआईपीएच-एच की प्रो. शैलजा तेताली, आईआईपीएच-एच के प्रो. सिरशेंदु चौधरी और स्टार हॉस्पिटल्स की डॉ. कृष्णवेनी येलमंचली जैसे पैनलिस्ट शामिल हुए। पैनल ने एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) के बढ़ते मुद्दे पर चर्चा की, खासकर वैश्विक यात्रा और व्यापार के संदर्भ में। उन्होंने एएमआर से निपटने के लिए विभागों के बीच सहयोग की तत्काल आवश्यकता पर चर्चा की और फेज थेरेपी जैसे अभिनव समाधान प्रस्तावित किए। पैनल ने एंटीबायोटिक के उपयोग पर सख्त नियमों और एएमआर से निपटने में वैश्विक सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया।
6. वन हेल्थ पहल में सामुदायिक सहभागिता
हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रो. जीवीआरके आचार्युलु की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र में आरआईसीएच की डॉ. सुष्मिता सुंदर, आईएमटी हैदराबाद के डॉ. के. श्रीहर्ष रेड्डी और एनआईआरडीपीआर की डॉ. सुचरिता पुजारी शामिल थीं। पैनल ने स्वास्थ्य संकटों, खासकर महामारी के दौरान प्रबंधन में सामुदायिक सहभागिता की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने चर्चा की कि कैसे सोशल मीडिया और जमीनी स्तर की पहल, जैसे कि महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रसारित करने और सक्रिय स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं। समुदायों को अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाना वन हेल्थ एजेंडा को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में पहचाना गया।
मुख्य बातें: वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण
संगोष्ठी ने वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए एक एकीकृत, बहुविषयक दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल दिया। विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा कि स्वास्थ्य को मानव, पशु या पर्यावरण के क्षेत्रों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और महामारी, एएमआर और जूनोटिक रोगों जैसे मुद्दों से निपटने के लिए सभी क्षेत्रों में सहयोग की आवश्यकता है।
- सामुदायिक सहभागिता और क्षमता निर्माण
एक मुख्य बात यह थी कि बीमारी की रोकथाम में सामुदायिक सशक्तिकरण की भूमिका क्या है। स्थानीय शासन संरचनाओं और नेटवर्क को मजबूत करना, जैसे कि महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के प्रसार और सक्रिय स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना गया।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और डेटा सिस्टम को मजबूत करना
संगोष्ठी ने विशेष रूप से जूनोटिक रोगों के लिए प्रकोप निगरानी में सुधार के लिए मजबूत सार्वजनिक स्थ्य अवसंरचना और वास्तविक समय डेटा सिस्टम की आवश्यकता को रेखांकित किया।
- एएमआर और सतत खाद्य सुरक्षा
एएमआर पर चर्चा ने एंटीबायोटिक उपयोग को विनियमित करने वाली वैश्विक नीतियों के महत्व पर जोर दिया, जबकि खाद्य सुरक्षा पैनल ने मानव पोषण, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय, जैविक खाद्य प्रणालियों की वकालत की।
- बदलती जलवायु में बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना
बच्चों के स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया, जिसमें सुरक्षित वातावरण के लिए बच्चों के अधिकारों को प्राथमिकता देने वाली नीतियों को सूचित करने के लिए साक्ष्य-आधारित शोध की मांग की गई।
वन प्लैनेट, वन हेल्थ, वन फ्यूचर संगोष्ठी एक मील का पत्थर कार्यक्रम था, जिसने वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहयोगात्मक, क्रॉस-सेक्टरल प्रयासों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। आईआईपीएच हैदराबाद लोगों, जानवरों और ग्रह के लिए स्थायी स्वास्थ्य समाधान बनाने के लिए अनुसंधान, शिक्षा और सामुदायिक जुड़ाव को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। साथ मिलकर, हम सभी के लिए एक स्वस्थ और अधिक लचीले भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं।
फोटो गैलरी
एनआईआरडीपीआर में यूनिकोड पर हिंदी कार्यशाला

हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान में प्रशिक्षण प्रबंधकों एवं युवा पेशेवरों के लिए यूनिकोड पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉ. ज्योतिस सत्यपालन, प्रोफेसर एवं प्रमुख (सीडीसी), श्री जयशंकर प्रसाद, उप निदेशक (राजभाषा) (सेवानिवृत्त), हिंदी शिक्षण योजना, तथा डॉ. उमेश, सहायक पुस्तकाध्यक्ष (सीडीसी) उपस्थित थे।
श्रीमती अनीता पांडे, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और श्री जयशंकर प्रसाद, उप निदेशक (राजभाषा) और डॉ. उमेशा एम.एल., सहायक पुस्तकाध्यक्ष, सीडीसी, एनआईआरडीपीआर का परिचय कराया, जो अतिथि वक्ता के रूप में उपस्थित थे और कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत की।
श्री जयशंकर प्रसाद, उप निदेशक (राजभाषा) ने ध्वनि टाइपिंग एवं पत्राचार की प्रक्रिया, अंग्रेजी से हिंदी तथा हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद प्रक्रिया के बारे में बताया तथा प्रतिभागियों को हिंदी में कार्य करने के लिए यूनिकोड का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के बारे में मार्गदर्शन दिया।
इसके अलावा, राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह के एक भाग के रूप में, डॉ. उमेश एम.एल. ने पुस्तकालय संसाधनों पर एक सत्र आयोजित किया, जिसमें विभिन्न संसाधन प्लेटफार्मों का व्यापक अवलोकन, शोध लेख डाउनलोड करने के लिए सुझाव और ग्रामरली जैसे उपकरणों की जानकारी साझा की गई।
कुल 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समापन डॉ. ज्योतिस सत्यपालन, प्रोफेसर और प्रमुख (सीडीसी) द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित करने के साथ हुआ। श्री ई. रमेश, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

एनआईआरडीपीआर, एनआईपीएचएम ने टॉलिक-2 अर्धवार्षिक बैठक का आयोजन किया
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) के तत्वावधान में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक-2) हैदराबाद की अर्धवार्षिक बैठक 28 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (एनआईपीएचएम), हैदराबाद में आयोजित की गई।

डॉ. ज्योतिस सत्यपालन, प्रोफेसर और अध्यक्ष (सीडीसी), एनआईआरडीपीआर ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर, एनआईपीएचएम के महानिदेशक डॉ. सागर हनुमान सिंह, एनआईपीएचएम की रजिस्ट्रार श्रीमती स्फूर्ति रेड्डी, आईआरएस; क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, बेंगलुरु (ऑनलाइन) के उप निदेशक (राजभाषा) डॉ. अनिरबन कुमार विश्वास; हिंदी शिक्षण योजना, सिकंदराबाद की उप निदेशक (राजभाषा) श्रीमती बेला; और एनआईआरडीपीआर की सहायक निदेशक (राजभाषा), श्रीमती अनीता पांडे, कार्यालय प्रमुख/कार्यकारी, हिंदी अनुवादक और विभिन्न कार्यालयों के अधिकारी शामिल हुए।

एनआईपीएचएम की रजिस्ट्रार श्रीमती स्फूर्ति रेड्डी ने मंच पर उपस्थित सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों का स्वागत किया। वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. चंद्रशेखर गुप्ता ने एनआईपीएचएम के बारे में हिंदी में विस्तृत पीपीटी प्रस्तुत की। क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, बेंगलुरु के उप निदेशक (ओ.एल.) डॉ. अनिरबन विश्वास ने हिंदी दिवस के अवसर पर दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना सहित राजभाषा विभाग की पहलों पर ऑनलाइन जानकारी दी। उन्होंने धारा 3(3), पत्राचार और अर्धवार्षिक रिपोर्ट भरने के बारे में भी मार्गदर्शन दिया।
एनआईपीएचएम के महानिदेशक डॉ. सागर हनुमान सिंह ने संस्थान द्वारा हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति पर प्रकाश डाला तथा कहा कि संस्थान राजभाषा विभाग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एनआईपीएचएम ने धारा 3(3) का पूर्णतः क्रियान्वयन किया है, सभी प्रशिक्षण पुस्तिकाओं का हिंदी में अनुवाद किया है तथा हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत नियमित रूप से कार्यशालाएं और प्रशिक्षण आयोजित करता है।
नराकास-2 की सदस्य सचिव श्रीमती अनीता पांडे ने शील्ड के लिए विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रस्तुत अर्ध-वार्षिक रिपोर्टों के मूल्यांकन के मानदंड साझा किए और सभी कार्यालयों से समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आग्रह किया।

डॉ. ज्योतिस सत्यपालन ने शील्ड प्राप्त करने वाले सभी कार्यालयों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने बताया कि टॉलिक-2 का उद्देश्य शहर में केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन से संबंधित समस्याओं का समाधान करना और इसके प्रयोग को बढ़ावा देना है। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान और पोल्ट्री अनुसंधान परियोजना को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शील्ड प्रदान की गई।
इसके अतिरिक्त, अतिथियों ने समिति की बैठकों की मेजबानी करने वाले नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति-2 के पांच आयोजन कार्यालयों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान किए।
हिंदी शिक्षण योजना की उपनिदेशक श्रीमती बेला ने प्रशिक्षण के महत्व पर बल दिया तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अधिक से अधिक नामांकन भेजने के लिए प्रोत्साहित किया।
अतिथियों ने टॉलिक-2 के सदस्य कार्यालय, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान द्वारा लिखित पुस्तक अर्पिश का विमोचन किया। यह पुस्तक किसानों, हितधारकों और छात्रों की सहायता के लिए तैयार की गई है।
बैठक का समापन एनआईपीएचएम के हिंदी अधिकारी श्री विजय कुमार शॉ द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। एनआईपीएचएम के हिंदी अनुवादक डॉ. मोहन राठौड़ और एनआईआरडीपीआर के वरिष्ठ हिंदी अनुवादक श्री ई. रमेश ने कार्यक्रम का संचालन किया। दोनों संस्थानों के राजभाषा अनुभाग में कार्यरत अधिकारियों और एनआईपीएचएम के अधिकारियों ने कार्यक्रम का समन्वय किया।
एनआईआरडीपीआर ने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने 1 नवंबर 2024 को स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। भारत सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रीय एकता शपथ में हिस्सा लिया।

अंग्रेजी और हिंदी में दिलाई गई शपथ का नेतृत्व एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता के महत्व पर प्रकाश डाला गया, जो सरदार पटेल के एकजुट भारत के स्थायी दृष्टिकोण को दर्शाता है।
सतत आजीविका के लिए महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अभिसरण के माध्यम से एनआरएम कार्यों को बढ़ावा देना

अन्य स्त्रोत व्यक्तियों के साथ प्रतिभागी
21 से 25 अक्टूबर 2024 तक वेज एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड्स सेंटर (सीडब्ल्यूईएल), एनआईआरडीपीआर ने ‘सतत आजीविका के लिए महात्मा गांधी नरेगा के तहत अभिसरण के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) कार्यों को बढ़ावा देने’ पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्देश्य महात्मा गांधी नरेगा के तहत दिशा-निर्देशों, प्रक्रियाओं और पहलों का पता लगाना और अभिसरण के माध्यम से एनआरएम और ग्रामीण आजीविका के बीच संबंधों पर चर्चा करना था, अन्य संबंधित विभागों के साथ एकीकृत एनआरएम योजनाओं का चित्रण करना। कुल मिलाकर, विभिन्न राज्यों में विभिन्न संगठनों से जुड़े 33 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

पहले दिन, विकास प्रलेखन एवं संचार केन्द्र के प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. ज्योतिस सत्यपालन ने महात्मा गांधी नरेगा और इसके अनुमेय कार्यों का अवलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन अनुमानों को संबोधित करते हुए शुरुआत की, जिसमें भारत की 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33-35% तक कम करने की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया। पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन में 120 देशों के साथ वैश्विक सौर गठबंधन की स्थापना में भारत की भूमिका का भी उल्लेख किया गया। डॉ. ज्योतिस ने महात्मा गांधी नरेगा के प्रमुख पहलुओं जैसे आजीविका सुरक्षा, रोजगार, संपत्ति निर्माण, विकेंद्रीकृत शासन और समावेशिता पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने एमजीएनआरईजीएस के तहत अनुमेय कार्यों के दायरे के बारे में विस्तार से बताया और ग्रामीण स्तर पर युवा विकास केंद्रों की अवधारणा पेश की।
सत्र 2 में, सीडब्ल्यूईएल के डॉ. अनुराधा पल्ला और श्री बिपिन कुमार ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा प्रस्तुत जीआईएस-आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) नियोजन उपकरण युक्तधारा-भुवन प्रस्तुत किया। उन्होंने नियोजन पोर्टल के विभिन्न चरणों का प्रदर्शन किया, जिससे प्रतिभागियों को जीआईएस-आधारित योजनाओं को सटीक रूप से विकसित करने के लिए ऑनलाइन उपकरण का उपयोग करने का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ। प्रतिभागियों ने इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया, उपकरण से स्वंय को परिचित किया और अपने-अपने राज्यों से संबंधित मामला अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए इसका उपयोग किया, जिसमें भू-टैग की गई ग्रामीण संपत्ति का प्रदर्शन किया गया।

तीसरे सत्र में, डॉ. अनुराधा पल्ला ने एक नया शैक्षणिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसे डीओपीटी मानकों के साथ संरेखित करने के लिए पायलट आधार पर लागू किया गया था। ‘महात्मा गांधी नरेगा के तहत श्रेणी-ए परिसंपत्तियों के माध्यम से आजीविका संवर्धन’ शीर्षक वाले सत्र का उद्देश्य प्रतिभागियों को नई शिक्षण पद्धति में शामिल करना था। प्रतिभागियों ने समूह चर्चाओं में भाग लिया, जहाँ राज्य के अधिकारियों ने जमीनी स्तर पर सामना किए जाने वाले मुद्दों की पहचान करने और एमजीएनआरईजीएस के तहत आजीविका संवर्धन रणनीतियों के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परिवर्तनों का प्रस्ताव करने के लिए सहयोग किया।

इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज (आईपीई) के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. श्रीधर राज ने ‘व्यवहार परिवर्तन और संचार कौशल’ पर एक सत्र लिया। इसमें प्रतिबद्धता जवाबदेही प्रदर्शन अवधारणाओं का महत्व शामिल था, जो जीवन में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण हैं। सत्र के दौरान, प्रतिभागियों के लिए संचार को बढ़ाने और सक्षमकर्ता, अक्षमकर्ता, प्रवर्तन, नियम/आदेश और पोस्टर/प्रदर्शन/संकेत बनाने के महत्व को दिखाने के लिए गतिविधियाँ आयोजित की गईं। प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया प्रदान करने के प्रभाव को दर्शाया गया, सकारात्मक परिणामों को बढ़ावा देने में इसके महत्व पर जोर दिया गया। पारस्परिक संबंधों की महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर प्रकाश डाला गया, जिला और ब्लॉक स्तरों पर हितधारकों और अधिकारियों के साथ प्रभावी सहयोग के लिए उनकी आवश्यकता को रेखांकित किया गया।
दूसरे दिन, डॉ. अनुराधा पल्ला ने “अभिसरण की अवधारणा” पर एक प्रस्तुति के साथ शुरुआत की, जिसमें कई विभागों में परियोजनाओं को लागू करने के लिए वास्तविक समय के परिदृश्यों और दृष्टिकोणों पर चर्चा की गई। उन्होंने जमीनी स्तर पर अभिसरण के प्रदर्शन और प्रभाव पर क्षेत्र के दौरे और शोध अध्ययनों के दौरान एकत्र किए गए विभिन्न राज्यों के मामला अध्ययनों पर प्रकाश डाला।
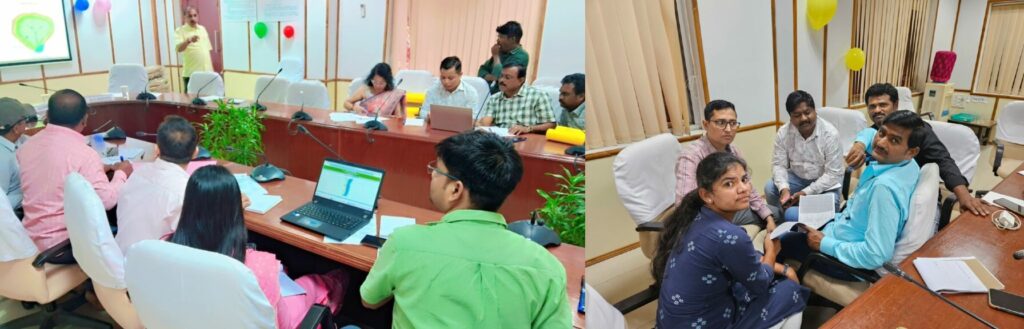
वर्षाधारित वन गठबंधन के पर्यावरण विशेषज्ञ श्री वी.आर. सौमित्री और डॉ. अनुराधा पल्ला ने महात्मा गांधी नरेगा के तहत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) और वाटरशेड पर सत्र संचालित किए । प्रतिभागियों ने संसाधनों और वाटरशेड कार्यों की पहचान करने के लिए समूह कार्य में भाग लिया और वाटरशेड कार्यों से जुड़े एसडीजी संकेतकों, वाटरशेड, जल स्रोत क्षेत्रों, बेसिन, जलग्रहण क्षेत्रों, उप-जलग्रहण क्षेत्रों, वाटरशेड, उप-वाटरशेड, माइक्रो वाटरशेड के संरक्षण की आवश्यकता का पता लगाया, जिसके बाद समूह प्रस्तुतियाँ हुईं।
सीडब्ल्यूईएल के पूर्व प्रमुख डॉ. जी. रजनीकांत ने ‘पीआरए तकनीक और व्यावहारिक अभ्यास’ पर एक सत्र आयोजित किया, जिसकी शुरुआत प्रतिभागियों को शामिल करने और ध्यान केंद्रित रखने के लिए सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) अभ्यास से हुई। उन्होंने जमीनी स्तर पर शोध करने के लिए आवश्यक तीन श्रेणियों में उपकरणों और तकनीकों के व्यापक स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। सत्र में सहभागी नियोजन प्रक्रियाओं को भी शामिल किया गया, जिसमें हितधारक पहचान, विश्लेषण, अधिकार और अपेक्षाएँ, और समूह गतिशीलता शामिल हैं। डॉ. रजनीकांत ने इन प्रक्रियाओं में प्रभावी संचार कौशल के महत्व पर जोर दिया।
तीसरे दिन प्रतिभागियों को विकाराबाद जिले के मोमिनपेट मंडल के गोविंदपुर गांव में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजना ‘रिज टू वैली कॉन्सेप्ट’ के बारे में जानकारी दी गई। ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने गांव की रूपरेखा, महात्मा गांधी नरेगा कार्यों की स्थिति और पूरी हो चुकी परियोजनाओं का अवलोकन कराया। प्रतिभागियों ने गांव के समुदाय से बातचीत की, जानकारी जुटाई और उनकी तुलना अपने राज्य की पद्धतियों से की। इस यात्रा से मूल्यवान जानकारी मिली और एक सफल एनआरएम पहल का प्रदर्शन हुआ जिसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है।

सामाजिक परियोजना केआईआईटी, भुवनेश्वर के निदेशक श्री सरोज कुमार दाश ने चौथे दिन ‘श्रम बजट का एकीकरण और ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ अभिसरण’ पर एक ऑनलाइन सत्र दिया। प्रतिभागियों ने मामला अध्ययन और सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए समूह चर्चा और प्रस्तुतियों में भाग लिया, जिसका मूल्यांकन डॉ. जी.वी. कृष्ण लोहिदास, सहायक प्रोफेसर ने किया। सत्र में गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकसित गांव, विकसित भारत के ढांचे के तहत श्रम बजट को जीपीडीपी के साथ एकीकृत करने पर जोर दिया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अभिसरण, दृष्टि संरेखण और सर्वोत्तम पद्धतियों के लिए रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया।

प्रतिभागियों को एनआईआरडीपीआर परिसर में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) ले जाया गया, जहाँ वरिष्ठ सलाहकार मोहम्मद खान ने “आजीविका बढ़ाने के लिए सतत ग्रामीण प्रौद्योगिकी” पर व्याख्यान दिया। उन्होंने आरटीपी में प्रदर्शित विभिन्न प्रौद्योगिकियों का अवलोकन प्रदान किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों को स्थानीय संसाधनों का लाभ उठाते हुए विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने और शहरी क्षेत्रों को इन उत्पादों के विपणन केंद्र के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया। सीआईएटीएंडएसजे के प्रमुख डॉ. सी. कथिरेसन ने भी सत्र के दौरान प्रतिभागियों से बातचीत की, जिससे ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने पर चर्चा को समृद्ध किया गया। मोहम्मद खान ने ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के महत्व पर जोर दिया, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों को स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके विनिर्माण केंद्र के रूप में देखने की दृष्टि पर प्रकाश डाला, जबकि शहरी क्षेत्र ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने और बेचने के लिए विपणन केंद्र के रूप में काम करते हैं।
पांचवें दिन की शुरुआत डॉ. अनुराधा पल्ला द्वारा ‘सामुदायिक लामबंदी और सामाजिक समावेश’ विषय पर एक सत्र के साथ हुई। प्रस्तुतियों में सामाजिक समावेश के महत्व और विभिन्न विभागों के साथ मिलकर एनआरएम कार्यों को लागू करने में उनकी सक्रिय भागीदारी पर प्रकाश डाला गया।
सीजीएआरडी, एनआईआरडीपीआर के डॉ. एनएसआर प्रसाद ने ‘पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी 2.0 योजना और निगरानी’ पर व्याख्यान दिया, जिसमें भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई (1.0 और 2.0) परियोजनाओं के प्रभाव पर जोर दिया गया। उन्होंने आईडब्ल्यूएमपी वाटरशेड की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और दृष्टि मोबाइल ऐप का अवलोकन प्रदान किया, जिसमें इसकी विशेषताएं, कार्यक्षमताएं और संस्करण शामिल हैं। डॉ. प्रसाद ने डब्ल्यूडीसी 2.0 में एनआरएससी की भूमिका पर चर्चा की और प्रतिभागियों को सृष्टि और दृष्टि ऐप से परिचित कराने के लिए उपयोगकर्ता पुस्तिकाएँ वितरित कीं। सत्र में एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के तहत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) और आजीविका गतिविधियों का भी प्रदर्शन किया गया।

डॉ. अनुराधा पल्ला ने महात्मा गांधी नरेगा के विभिन्न सर्वोत्तम अभ्यासों और फील्ड प्रस्तुतियों की जॉंच की, और सभी प्रतिभागियों के बीच समूह चर्चा आयोजित की गई। समूह प्रस्तुति गतिविधि आयोजित की गई, जहाँ प्रशिक्षण प्रतिभागियों ने अपने चार्ट प्रस्तुत किए और गोविंदपुर गाँव-रिज टू वैली परियोजना के क्षेत्र दौरे के दौरान अपने अवलोकनों को समझाया।
सीडब्ल्यूईएंडएल के सहायक प्रोफेसर डॉ. जी.वी. कृष्ण लोहिदास ने ‘महात्मा गांधी नरेगा के तहत साझा संपत्ति संसाधन प्रबंधन’ पर एक सत्र संचालित किया। प्रस्तुति में सामाजिक समानता पर ध्यान केंद्रित किया गया और कार्य में शामिल सभी लोगों को अभिसरण के तहत कार्यों के निष्पादन के लिए सभी विभिन्न विभागों की ओर से ध्यान केंद्रित करने का मौका दिया गया।
समापन सत्र के दौरान, प्रतिभागियों ने शिक्षण पद्धति की सराहना की तथा बताया कि किस प्रकार इसने उनके कौशल, ज्ञान और समग्र शिक्षण अनुभव को प्रभावी ढंग से बढ़ाया।
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज में उत्कृष्टता का एक प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन-ईएससीएपी उत्कृष्टता केंद्रों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त, यह प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श की अंतर-संबंधित गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण विकास पदाधिकारियों, पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों, बैंकरों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों की क्षमता का निर्माण करता है। यह संस्थान तेलंगाना राज्य के ऐतिहासिक शहर हैदराबाद में स्थित है। एनआईआरडीपीआर ने 2008 में अपनी स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया। हैदराबाद में मुख्य परिसर के अलावा, इस संस्थान का गुवाहाटी, असम में एक उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र, नई दिल्ली में एक शाखा और वैशाली, बिहार में एक कैरियर मार्गदर्शन केंद्र है।

















